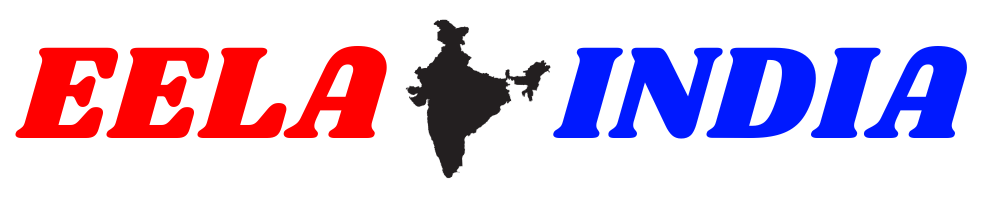जात से बनेगी बात, जानिए क्याहै इसका इतिहास और कैसे बना राजनीतिक मुद्दा
EELA INDIA
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता वाली राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCPA) ने आगामी जनगणना (Census) में जातिगत जनगणना (Caste Census) को मंजूरी दे दी है। एक तरह से कई दशकों पुरानी मांग को ना-नुकुर के बाद NDA सरकार ने मान लिया। सरकार ने इस मुद्दे पर चार साल पहले संसद में औपचारिक रूप से व्यक्त की गई अपनी राय बदल ली।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 30 अप्रैल को निर्णय की घोषणा करते हुए कहा, “जातिगत जनगणना हमारे समाज की सामाजिक और आर्थिक संरचना को मजबूत करेगी।” इस एलान के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने हमारी मांग मान ली है और हम इसके समर्थन में हैं।
उल्लेखनीय है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी ने इसे अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के साथ मुद्दा बना लिया था। हालांकि सत्तारूढ़ दल भाजपा के नेताओं ने इसे पहले देश तोड़ने वाली मांग बताया था।
सरकार के अचानक रुख बदलने से लगता है कि यह शायद चुनावी लाभ के नजरिये से हुआ है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह गणना कब शुरू होगी, कब तक चलेगी और किस स्वरूप में की जाएगी।
आखिर क्या है जातिगत जनगणना (Caste Census)
जातिगत जनगणना ( Caste Census), राष्ट्रीय जनगणना (Census) के दौरान व्यक्तियों के दौरान व्यक्तियों की जातियों पर व्यवस्थित आंकड़ों का संग्रह है। भारत में, जहां जाति ने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता को आकार दिया है, ऐसे आंकड़े जनसांख्यिकीय वितरण, सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और विभिन्न जाति समूहों के प्रतिनिधित्व के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल विभिन्न कार्यक्रमों में आरक्षण और सामाजिक न्याय पर नीतियों को सूचित करने के लिए किया जा सकता है।
लंबा इतिहास
बिटिश भारत (1881-1931): ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने 1881 और 1931 के बीच हर दशक में आयोजित जनगणना में जाति गणना को शामिल किया। इन सर्वेक्षणों ने विस्तृत जनसांख्यिकीय आंकड़े प्रदान करते हुए जनसंख्या को जाति, धर्म और व्यवसाय के आधार पर वगीकृत किया। यह कदम आंशिक रूप से भारत की जटिल सामाजिक संरचना को समझने और उस पर शासन करने की औपनिवेशिक आवश्यकता से प्रेरित था।
स्वतन्त्रता के बाद बदलाव (1951)
वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, 1951 में आजाद भारत की पहली जनगणना ने एक महत्त्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर जाति गणना को बंद करने का फैसला किया। यह निर्णय इस विश्वास पर आधारित था कि जाति पर ध्यान केंद्रित करने से विभाजन को बढ़ावा मिल सकता है और एक नए स्वतंत्र राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
1961 का निर्देश
एक दशक बाद, 1961 में, केंद्र सरकार ने राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग की राज्य-विशिष्ट सूचियां तैयार करने के लिए अपने स्तर से सर्वेक्षण कराने की अनुमति दी। यह कदम अनुसूचित जाति और जनजाति से परे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए कल्याणकारी कदमों की मांग के जवाब में था। हालांकि, कोई राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना नहीं की गई थी।
जातिगत जनगणना कैसे बनी राजनीतिक मुद्दा
साल 1980 में केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी के लिए 27 फीसद आरक्षण प्रदान करने की मंडल आयोग की सिफारिश ने जाति को फिर से राजनीतिक चर्चा में ला दिया। जाति संबंधी व्यापक आंकड़ों की कमी ने ओबीसी आबादी की सही पहचान और मात्रा निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण बना दिया, जिससे जातिगत जनगणना की मांग बढ़ गई।
सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011
वर्ष 2011 में, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार ने सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (Socio Economic Caste Census) करवाई, जो 1931 के बाद से देश भर में जाति के आंकड़े एकत्र करने का पहला प्रयास था। हालांकि, SECC 2011 के आंकड़ों को कभी भी पूरी तरह से जारी या उपयोग नहीं किया गया, जिसके कारण विपक्षी दलों और जाति-आधारित संगठनों ने इसकी आलोचना की।
राज्य स्तरीय पहल
राष्ट्रीय जातिगत जनगणना के अभाव में, बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों ने हाल के वर्षों में अपने-अपने यहां जाति सर्वेक्षण कराए हैं। इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य राज्य-विशिष्ट आरक्षण नीतियों और कल्याण कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए आंकड़े एकत्र करना था। 2023 में बिहार के जाति सर्वेक्षण से पता चला कि ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) राज्य की आबादी का 63 फीसद से अधिक हिस्सा हैं।
क्यों मायने रखती है जातिगत जनगणना
जातिगत जनगणना एक जनसांख्यिकीय कवायद से कहीं अधिक है। यह गहरे सामाजिक निहितार्थों वाला राजनीतिक रूप से एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। विशेषज्ञों ने कहा है कि जनगणना में जाति को शामिल करने से आरक्षण नीतियों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय पहल पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। यह चुनावी रणनीतियों को भी नया रूप दे सकता है, क्योंकि पार्टियां समर्थन पाने की होड़ में लगी रहती हैं।