विश्वगुरु बनने की राह: निर्णय, दिशाएं और दुविधाएं
राजनीति (Politics) महज़ सत्ता का खेल नहीं है यह राज्य के निर्माण संचालन और भविष्य की दिशा तय करने वाला वह निर्णायक यंत्र है जिसके हर फैसले में एक राष्ट्र (Nation) की नियति छिपी होती है। राजनीतिक निर्णय कभी-कभी युद्ध शांति, समृद्धि या पतन के रूप में सामने आते हैं। चाहे किसी भी युग की बात करें राज्य का जन्म और उसका संचालन उसी निर्णय से संभव होता है जो उस वक्त की राजनीति तय करती है।
आज जब हमारे प्यारा देश ‘विश्वगुरु’ बनने का सपना देख रहा है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है तब यह जरूरी हो जाता है कि हम यह समझें कि इन सबके मूल में कौन-से राजनीतिक निर्णय हैं और वे हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं।
राजनीतिक निर्णय: राज्य का मूल आधार
राज्य का अस्तित्व केवल भूगोल से नहीं बल्कि निर्णय लेने की क्षमता से होता है। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी अनुकूल क्यों न हों यदि नेतृत्व निर्णायक नहीं है तो राज्य केवल कागज़ी ढाँचा बनकर रह जाएगा। हिंदुस्तान जैसे विशाल और विविधताओं वाले देश में यह निर्णय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
ये भी पढ़ें- ये भी पढ़ें- अगर हवाई हमला हो जाए तो क्या करें, भारत-पाक तनाव में जान बचाने की टिप्स यहां जानें
राजनीतिक दलों का उदय और उनकी भूमिका यहाँ केंद्रीय बन जाती है परन्तु यह भी ध्यान देने योग्य है कि वे राज्य नहीं होते बल्कि राज्य की नीतियों को प्रभावित करने वाली इकाइयाँ होती हैं। जब कोई दल अपनी विचारधारा को ही राज्य का पर्याय बना देता है तब लोकतंत्र के संतुलन में दरारें पड़ने लगती हैं।
जीरो टॉलरेंस की नीति और उसकी गहराई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने ‘आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस’ (Zero tolerance Policy against terrorism) की नीति को राजनीतिक निर्णय का रूप दिया। प्रारंभ में यह नीति पाकिस्तान की आतंकवाद पोषित गतिविधियों के खिलाफ एक आक्रामक कूटनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण के रूप में देखी गई। मगर जब इस नीति का अनुप्रयोग हिंदुस्तान के भीतर की असहमति विरोध और वैचारिक मतभेदों पर होने लगा तब यह निर्णय एक खतरनाक मोड़ लेने लगा।
‘नक्सल’ ‘शहरी माओवादी’ और ‘राष्ट्रविरोधी’ जैसे लेबल विपक्षी आवाजों पर चस्पा किए जाने लगे। यह वह बिंदु था जहाँ राज्य और दल के बीच की रेखा धुंधली हो गई। राजनीतिक निर्णयों की वैधता तब तक ही स्वीकार्य रहती है जब तक वे राज्य के संविधानिक ढाँचे के भीतर हों।
राजनीति में धर्म का समावेश और परिणाम
बीते वर्षों में हिंदुस्तान की राजनीति में ‘सनातन धर्म’ को राष्ट्र की परिभाषा में शामिल करने का प्रयास हुआ है। यह एक गहरा राजनीतिक निर्णय था जिसमें बहुसंख्यक पहचान को केंद्र में रखकर अल्पसंख्यकों दलितों और वंचित वर्गों को हाशिए पर डाल दिया गया। जाति व्यवस्था की आलोचना को अपराध की तरह देखा जाने लगा और हिंदुस्तान का सार्वजनिक विमर्श धार्मिक प्रतीकों में बँधता चला गया।
ये भी पढ़ें- ये भी पढ़ें- जानें सीजफायर क्या है और भारत-पाकिस्तान के बीच इसका क्या मतलब
इस राजनीतिक निर्णय ने भारतीय समाज को सांस्कृतिक स्तर पर विभाजित कर दिया और राज्य की नीतियाँ अब एक विचारधारा विशेष की पक्षधर लगने लगीं। इसका असर केवल आंतरिक नीति तक सीमित नहीं रहा बल्कि विदेश नीति में भी यह नजर आने लगा।
भारत की आक्रामक विदेश नीति: अकेलापन बढ़ता गया
हिंदुस्तान की पाकिस्तान और चीन से सीमा पर तनातनी कोई नई बात नहीं मगर हालिया सैन्य निर्णय और नदियों का जल रोकने जैसे कदम भारत की पारंपरिक विदेश नीति से अलग थे। मोदी सरकार ने इजरायल की तरह तेज़ी से प्रतिक्रिया देने की नीति अपनाई मगर भारत की भौगोलिक और कूटनीतिक स्थिति इजरायल से कहीं अधिक कठिन है।
यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह रहा कि भारत ने जो निर्णय लिए उनके पीछे अंतरराष्ट्रीय समर्थन का आकलन अधूरा रहा। न तो मित्र शक्तियाँ खुलकर सामने आईं और न ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोई निर्णायक हस्तक्षेप किया। राजनीतिक निर्णय को रणनीतिक सहयोग की समझदारी से अलग कर देखना भारत को एक ऐसी स्थिति में पहुँचा गया जहाँ वह अकेला दिखने लगा।
‘आतंकवाद’ की वैश्विक परिभाषा और भारत का रुख
‘आतंकवाद’ (Terrorism) एक बहुआयामी शब्द है। आधुनिक वैश्विक राजनीति में इसे अमेरिका ने धर्मयुद्ध की अवधारणा से जोड़ दिया और इसे इस्लाम के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया। भारत में भाजपा ने इसी अवधारणा को अपनी घरेलू नीति में ढालकर आतंकवाद को केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक विरोध के प्रतीकों से भी जोड़ दिया।
यह निर्णय भारत के लोकतांत्रिक चरित्र पर सीधा प्रहार था। विरोधी आवाजों को राष्ट्रविरोधी करार देना और जनता के एक हिस्से को डराकर चुप कराना एक लंबी लोकतांत्रिक परंपरा वाले देश के लिए खतरनाक संकेत था।
मीडिया ट्रोल्स और युद्ध का कारोबार
आज की राजनीति में मीडिया भी एक राजनीतिक हथियार बन चुका है। जब सरकार युद्ध की ओर कदम बढ़ाती है तो राष्ट्रीय मीडिया विजय का जयघोष करने लगता है। आलोचना को देशद्रोह और सवाल उठाने को कायरता कह दिया जाता है। युद्ध को एक मनोरंजन और गर्व के क्षण में बदल दिया जाता है।
ये भी पढ़ें- ये भी पढ़ें- छोटे दल, बड़ी बात; बिहार में इंडिया गठबंधन का बिगड़ सकता है खेल
ट्रोल्स सेना के नाम पर किसी भी सवाल उठाने वाले को गालियाँ देने लगते हैं और इस प्रकार जनमत को नियंत्रित किया जाता है। यह राजनीतिक निर्णय एक राष्ट्र के भविष्य को कितनी दूर तक प्रभावित करता है इसका मूल्यांकन केवल युद्ध के आँकड़ों से नहीं बल्कि सामाजिक विभाजन और कूटनीतिक अलगाव से करना चाहिए।
भूगोल के दरवाज़े: पाकिस्तान अमेरिका और चीन
भारत की विदेश नीति को लेकर एक अहम बिंदु है—उसका भूगोल। पाकिस्तान न केवल भारत का पड़ोसी है बल्कि चीन और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों की रणनीतिक महत्वाकांक्षा का हिस्सा भी है। जिस वक्त भारत खुद को विश्वगुरु बताने में लगा था उसी वक्त पाकिस्तान चीन के लिए मध्य एशिया में प्रवेश का मुख्य द्वार बन गया था।
भारत का यह समझना जरूरी था कि वैश्विक मंच पर उपस्थिति केवल भाषणों और घोषणाओं से नहीं बल्कि रणनीतिक गहराई और साझेदारियों से तय होती है। चीन की बढ़ती उपस्थिति ने भारत के लिए विदेश नीति को कहीं अधिक कठिन बना दिया है।
खड़े हो रहे हैं ये सवाल
अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत की राजनीति अपने निर्णयों की समीक्षा करेगी। क्या अन्य राजनीतिक दल विकल्प देने में सक्षम हैं। कांग्रेस अब भी अतीत के गौरवमयी पलों की स्मृतियों में खोई हुई है। वामपंथ और क्षेत्रीय दल विकल्प तो दे रहे हैं मगर उनका प्रभाव सीमित है।
राजनीतिक निर्णय केवल चुनाव जीतने की रणनीति नहीं होते। वे राष्ट्र के भविष्य के स्वरूप को गढ़ते हैं। इसलिए जरूरी है कि राजनीतिक दल अपनी विचारधारात्मक कठोरता छोड़कर देश की जनता और उसकी वास्तविक समस्याओं के संदर्भ में निर्णय लें।
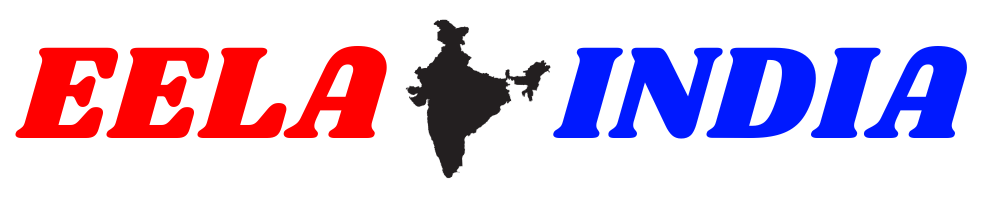









Pingback: किंगमेकर की तलाश में बिहार, क्या जाति आधारित गणना बदलेगी सत्ता का समीकरण